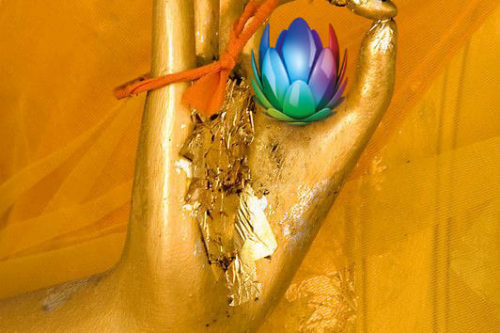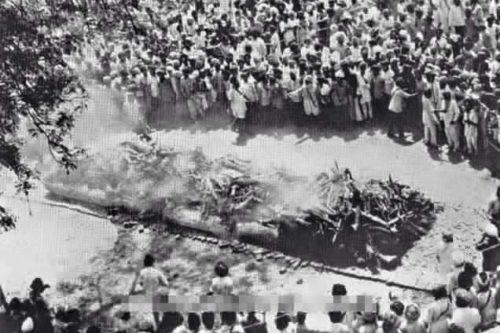अन्न भोजन है, भोजन जीवन है,
यह सार्वभौम सत्य है.
परंतु आध्यात्मिकता के प्राचीनतम चरम उपदेशकों में परिगणित उपनिषद ग्रंथों से एक तैत्तिरीयोपनिषद् की उक्ति है-
“अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।”
अर्थ है-
अन्न ब्रह्म है, क्योंकि ऐसा ही जाना जाता है।
अन्नं ब्रह्म है, व्यंजन होने से नहीं, व्यजान होने से.
अन्न से प्राण है, प्राण से प्राणी, उनसे ही ब्रह्म,
सो पहले स्तर पर तो ब्रह्म यही है.
अन्न देह की जरूरत ही नहीं, देह भी है,
वह पंचकोश में से अन्नमय कोश बनाता है।
आगे जो भी चिन्मय है, उसकी नींव पर खड़ा है.
विज्ञान के जगत् में चलते हैं।
यह जानना रुचिर है कि
लगभग सभी अनाज मूलतः घास हैं.
घास पादप जगत् की वह प्रजाति है,
जिसके पत्ते तने से निकलते हैं और पत्तों में रेशे सीधे ही छोर तक जाते हैं।
इस प्रकार से हम आज भी घास पर ही जीवित हैं.
अनाज के लिए संस्कृत में धान्य शब्द है,
जो लोकभाषा में आकर धान बन गया.
धीरे-धीरे यह लोकभाषा में उस क्षेत्रविशेष के प्रमुख अन्न के लिए प्रयुक्त हो गया.
जैसे उत्तर मध्य भारत में धान मूलतः चावल की फसल है,
तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की और दक्षिणी राजस्थान में मक्के की.
संस्कृत में व्रीहि भी अन्नवाचक है।
वह बहुव्रीहि समास भी है।
उसका अर्थ है, बहुत या बहुत तरह के अनाज वाला.
अनाजों की विविधता बमुश्किल दर्जन भर तक सिमटी है-
चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, मडुआ(रागी), सावाँ (श्यामाक), रामदाना (राजगिरा) आदि तक.
इनमें भी पहले दो चार तक ही समाज सिमट चुका है, बाद की चीजें या तो व्रत के लिए रख ली गई हैं, या मोटा अनाज मान कर दरकिनार की जा चुकी हैं।
इनके इतिहास पर कुछ दृष्टिपात करते हैं-
चावल कृषि में आए कुछ सबसे पहले अनाजों में से है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या चावलभोजी ही है।
चावल के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त राइस शब्द मूलतः तमिल भाषा के “अरिसी” शब्द से बना है। अनाजों में यह सर्वाधिक विविधता भरा अनाज है। दुनिया भर में इसकी लगभग एक लाख से अधिक प्रजातियाँ रही हैं। International Rice Gene Bank के अंतर्गत 90 हजार प्रजातियों के जेनेटिक सैंपल रखे गए हैं, जिनमें 40 हजार तक अनाज के रूप में हैं. यह भी उसके विविधता भरे विस्तार का एक अंश भर है। इनमें हर प्रजातिय के चावल का अपना अनूठापन है-
कुछ अंगुल भर लंबे दाने के, तो कुछ जीरे की तरह छोटे व महीन, कुछ गेहूँ व जौ से भी मोटे, तो कुछ तिनके से पतले. कुछ मोती से भी धवल, तो कुछ माणिक से लाल. कुछ चिपकने वाले, कुछ बिल्कुल विलग फरहरे. पर संपन्न होती दुनिया में सब बस बासमतीमय हो गया है। वह लाख रूपों वाले चावल का लाखवाँ अंश ही तो है। अब हर व्यंजन पुलाव, ताहिरी या बिरयानी तो हो नहीं सकता. रोज के भात के लिए अलग चाहिए, खिचड़ी के लिए अलग, खीर, पासम् और फिरनी के लिए अलग.
यह जानना रुचिर है कि आज अलाउंस के लिए प्रयुक्त होने वाला भत्ता शब्द “भात” (संस्कृत में भक्तम्) शब्द से बना है। माना जाता है कि मौर्य काल में सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त भोजन के लिए अलग से मानदेय व्यवस्था थी, जो कालांतर में अर्थ विस्तार पाकर अलाउंस के लिए प्रयुक्त होने लगा.
जौ व मक्का विश्व के सबसे पुरातन कृषि अनाजों में हैं,
भारत में जौ व शेष विश्व में मक्का प्रमुख था. जौ वैदिक काल में “यव” कहा जाता था और इससे बने व्यंजनों में यवागू सबसे प्रसिद्ध था, जो जौ का दलिया, खीर, हलवा या लापसी में कुछ भी हो सकता था। इसके सत्तू, लड्डू, राब, आदि आज तक प्रसिद्ध रहे हैं।
गेहूँ का प्रवेश बहुत बाद में हुआ. संस्कृत में गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है- गाय को धुआँ करना. यह इस अर्थ में इसकी अन्नपरक महत्ता नहीं बताता. विचारक मानते हैं कि लगभग 8 हजार साल पहले पशुचारकों या आक्रमणकारियों के साथ मध्य एशिया की goat grass (Aegilops tauschii) का भारत के जंगली गेहूँ (T. dicoccoides) से मिलन होकर आज के 42 गुणसूत्र वाले खाद्य गेहूँ का विकास हुआ। तब से आज तक इसका ऐसा साम्राज्य है कि विश्व की एक तिहाई से अधिक आबादी की आजीविका और हमारे भोजन के का 20 प्रतिशत से ज्यादा कैलोरी इस अकेले अनाज से आती है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि रोटी, चकला, बेलन के लिए पुरातन संस्कृत में शब्द नहीं है, जिससे भी इसके बाद में आने का पता चलता है।
बाजरे को लेकर उसके मूल के संबंध में दो दावे हैं- अफ्रीका व एशिया, जिसमें अधिकांश विचारक अफ्रीका को मानते हैं। वह भारत में बाजरा व बाजरी दो रूपों में मिलता है। पहला जरा बड़ा है, दूसरा जरा छोटा और अधिक स्वादिष्ट भी. अंग्रेजी में इसे पर्ल मिलेट कहते हैं, अर्थात् मोती सा अन्न. यह प्रोटीन व ऑयरन से भरपूर है और रेगिस्तान का प्राण रहा है।
ज्वार अपने रंग रूप में बहुत कुछ बाजरे सा रहा है। पर यह अब भोजन में कम ही प्रयुक्त होता है। यह भी वैसी ही गुणवत्ता व तासीर का रहा है। चारे में यह चरी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।
कोदो व मडुआ लगभग एक ही अन्न से हैं. इनमें तो ज्वार-बाजरा या जौ-गेहूँ का सा भी अंतर नहीं दिखता.
दोनों लगभग विलुप्ति की ओर जाकर वापस लौट रहे हैं।
कोदो संभवतः “कदन्न” से बना है। मोटे अनाज में होने के कारण उसे ऐसा कहा गया. मडुआ अब रागी के नाम से पुनः लोकप्रिय हो रहा है।
सावाँ (श्यामाक), रामदाना (राजगिरा) आदि आधे अनाज माने जाते हैं, विज्ञान की भाषा में इन्हें Pseudo-Cereal भी कहा जाता है। प्रायः ये व्रत के भोजन माने जाते हैं। खीर, हलवा, कचौरी आदि के रूप में ये अपनी व्यंजना प्रस्तुत करते हैं।
भोजन हमारा धर्म व धर्म का इतिहास भी बताता है।
युगों से युगधर्म जन्मते हैं
और
युगधर्म से ये देवत्व-
-कभी शिवत्व
-कभी शक्तिमत्ता
-कभी विष्णुमय
तो
-कभी ब्रह्मविद्
विकासवादी धर्मदर्शन में माना जाता है कि
जिस देवता को भोग हेतु जो सामग्री अर्पित की जाती है,
उससे पता चलता है कि
उनकी पूजा मूलतः कब प्रारंभ या प्रमुख हुई होगी।
माना जाता है कि सरकार
जब आहारसंग्राहक युग था,
तब शिव आराध्य बने,
इसी कारण शिव की पूजा में अकृष्य भोग हैं-
मंदार पुष्प, धतूरा, भाँग, दूध.
जब आखेटक युग हुआ,
तब काली आराध्य बनीं,
इसी कारण उनकी सेवा पूजा में बलि है, सुरा है, तंत्र है.
राजतंत्रों के अभेद्य दुर्गों का दुर्गा वही बनी रहीं.
जब कृषि व पशुपालन का युग आया,
तो विष्णु आये,
गोपालक कृष्ण बनकर.
उनको चढ़ाई जाने वाली समस्त सामग्री कृषि युग की है।
गेहूँ के चूर्ण से लेकर हलवा, पूड़ी, खीर, लड्डू तक.
राजतंत्रों के युग ने ईश्वर को राजा की तरह चित्रित करना शुरू कर दिया.
लड्डू विनायक गणेश तक है।
वे भी पौराणिक युग में ही मंगलमूर्ति बने,
कृषि युग तब तक शिखरस्थ हो चुका था।
जैसे लोग होंगे, वैसे ईश्वर होंगे,
जैसा युग होगा, वैसी देवी होंगी.
अकालों के युग में अन्नपूर्णा, संतोषी और शाकंभरी की कल्पना व प्रार्थना प्रबल होती रही हैं.
भोजन की बात चले,
तो अनजाने ही धर्म के जगत् से तमाम मिथक व कथाएँ स्मृत हो आती हैं-
उनमें राम के आगे रखे शबरी के बेर हों,
या कृष्ण के सामने रखे विदुर पत्नी के केले के छिलके,
या फिर उनके द्वारा गोपों संग चुरा कर खाये गए गोपियों के दधि-मक्खन.
महावीर के लिए चंदनबाला के द्वारा लाई गई उड़द की दाल हो,
या फिर बुद्ध के समक्ष रखी सुजाता की खीर.
जीसस द्वारा सलीब पर जाने से पहले शिष्यों को दिया गया लास्ट सपर हो,
या नानक द्वारा तोलते समय तेरह आने पर “तेरा तुझको अर्पण” के रूप में कर दिया गया दान.
और जबकि अन्न को ही जोड़ कर व्यंजन बनाने का मेला लग रहा है,
तब अनायास पुन: अभिव्यक्त हो ही जाता है,
“तेरा तुझको अर्पण”
—————————
संदर्भित मंत्र-
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।
अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।
अन्नेन जातानि जीवन्ति।
अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।
—तैत्तिरीयोपनिषद् , भृगुवल्ली-1